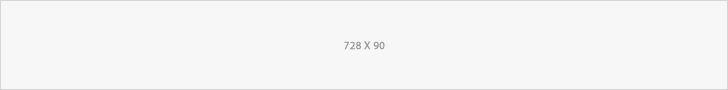आजादी के बाद से हमारे देश में कितना कुछ बदल गया है। समाज, विचार, रहन-सहन, आबोहवा, सभी में बदलाव आया है। बस, नहीं बदला, तो हमारे जनप्रतिनिधियों का रवैया या यूं कहें कि हमारे जनप्रतिनिधि बदलना ही नहीं चाहते। वे आज भी उतने ही मतलबी हैं, जितने पहले हुआ करते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले उनका मंतव्य देशहित में होता था, आज स्वयं के हित में होता है। वैसे भी राजनीति के हमाम में तमाम राजनीतिक दल नंगे हैं और जहां उनकी सियासत को खतरा पैदा होता है वे पूर्वाग्रहों व विचारधाराओं के परे हमेशा से एक होते रहे हैं। फिर चाहे वह नेताओं को प्राप्त होने वाली सुविधाओं की बात हो या हाल ही में देश के सर्वोच्च न्यायालय के अहम आदेशों के पालन का मसला हो। गौरतलब है कि अपराधियों के चुनाव लड़ने पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक और राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के दायरे में लाने के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश के खिलाफ पूरी सियासत एकजुट हो गई है। संसद के मानसून सत्र में इन दोनों फैसलों के खिलाफ विधेयक लाकर उन्हें रद करने की तैयारी हो गई है। साफ है कि भ्रष्टाचार और अपराधीकरण से राजनीतिक दल खुद को मुक्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। सरकार ने जिस कानून को जनता के हाथ में ताकत देने का सबसे बड़ा हथियार बताया था, वह अब उसी से डर गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने तय किया है कि राजनीतिक दलों को आरटीआई कानून के दायरे में आने से रोकने के लिए इस कानून में संशोधन किया जाएगा। सरकार इस मामले पर सभी पार्टियों की राय पहले ही ले चुकी है। मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने भी इस कानून में संशोधन के सरकार के प्रस्ताव को संसद में समर्थन देने का भरोसा दिलाया है। इस मामले में लगभग सभी राजनीतिक दलों की एक राय है। हाल में एक मामले की सुनवाई के दौरान केंद्रीय सूचना आयोग ने तय किया था कि सभी छह पार्टियां जिन्हें चुनाव आयोग से राष्ट्रीय दल की मान्यता मिली हुई है, वे इस कानून की परिधि में आते हैं। कांग्रेस, भाजपा, माकपा, भाकपा, बसपा और राकांपा राष्ट्रीय दल हैं। इनमें सिर्फ भाकपा ने इस आदेश का सम्मान करते हुए आरटीआई आवेदन के जवाब में सूचना मुहैया करवाई और पार्टी में लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया। हालांकि इस मामले में राजनीतिक दलों की दलील है कि वे सार्वजनिक संस्थाएं नहीं हैं लिहाजा वे आरटीआई के दायरे में नहीं आते हैं। वहीं राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं का यह भी मानना है कि दलों की जिम्मेदारी नीति को लेकर आम लोगों के प्रति है न कि किसी संस्था के प्रति। कुछ का मानना है कि जब राजनीतिक दलों के कामकाज की निगरानी के लिए चुनाव आयोग है तब नई संस्था का क्या औचित्य? हालांकि राजनीतिक दलों के तर्कों से आम आदमी का सहमत होना आवश्यक नहीं है किन्तु उनकी इस धूर्तता पर किसी को ख़ास अचरज भी नहीं हुआ है।
आजादी के बाद से हमारे देश में कितना कुछ बदल गया है। समाज, विचार, रहन-सहन, आबोहवा, सभी में बदलाव आया है। बस, नहीं बदला, तो हमारे जनप्रतिनिधियों का रवैया या यूं कहें कि हमारे जनप्रतिनिधि बदलना ही नहीं चाहते। वे आज भी उतने ही मतलबी हैं, जितने पहले हुआ करते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले उनका मंतव्य देशहित में होता था, आज स्वयं के हित में होता है। वैसे भी राजनीति के हमाम में तमाम राजनीतिक दल नंगे हैं और जहां उनकी सियासत को खतरा पैदा होता है वे पूर्वाग्रहों व विचारधाराओं के परे हमेशा से एक होते रहे हैं। फिर चाहे वह नेताओं को प्राप्त होने वाली सुविधाओं की बात हो या हाल ही में देश के सर्वोच्च न्यायालय के अहम आदेशों के पालन का मसला हो। गौरतलब है कि अपराधियों के चुनाव लड़ने पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक और राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के दायरे में लाने के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश के खिलाफ पूरी सियासत एकजुट हो गई है। संसद के मानसून सत्र में इन दोनों फैसलों के खिलाफ विधेयक लाकर उन्हें रद करने की तैयारी हो गई है। साफ है कि भ्रष्टाचार और अपराधीकरण से राजनीतिक दल खुद को मुक्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। सरकार ने जिस कानून को जनता के हाथ में ताकत देने का सबसे बड़ा हथियार बताया था, वह अब उसी से डर गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने तय किया है कि राजनीतिक दलों को आरटीआई कानून के दायरे में आने से रोकने के लिए इस कानून में संशोधन किया जाएगा। सरकार इस मामले पर सभी पार्टियों की राय पहले ही ले चुकी है। मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने भी इस कानून में संशोधन के सरकार के प्रस्ताव को संसद में समर्थन देने का भरोसा दिलाया है। इस मामले में लगभग सभी राजनीतिक दलों की एक राय है। हाल में एक मामले की सुनवाई के दौरान केंद्रीय सूचना आयोग ने तय किया था कि सभी छह पार्टियां जिन्हें चुनाव आयोग से राष्ट्रीय दल की मान्यता मिली हुई है, वे इस कानून की परिधि में आते हैं। कांग्रेस, भाजपा, माकपा, भाकपा, बसपा और राकांपा राष्ट्रीय दल हैं। इनमें सिर्फ भाकपा ने इस आदेश का सम्मान करते हुए आरटीआई आवेदन के जवाब में सूचना मुहैया करवाई और पार्टी में लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया। हालांकि इस मामले में राजनीतिक दलों की दलील है कि वे सार्वजनिक संस्थाएं नहीं हैं लिहाजा वे आरटीआई के दायरे में नहीं आते हैं। वहीं राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं का यह भी मानना है कि दलों की जिम्मेदारी नीति को लेकर आम लोगों के प्रति है न कि किसी संस्था के प्रति। कुछ का मानना है कि जब राजनीतिक दलों के कामकाज की निगरानी के लिए चुनाव आयोग है तब नई संस्था का क्या औचित्य? हालांकि राजनीतिक दलों के तर्कों से आम आदमी का सहमत होना आवश्यक नहीं है किन्तु उनकी इस धूर्तता पर किसी को ख़ास अचरज भी नहीं हुआ है।
वहीं दूसरी ओर जेल से चुनाव लड़ने पर रोक और दो साल से ज्यादा सजा होने पर सदन की सदस्यता स्वत: खत्म होने वाले सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले के खिलाफ संसद के मानसून सत्र में विधेयक लाने के लिए भी सरकार तैयार है। मानसून सत्र के सुचारु संचालन के उद्देश्य से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में राजनीति का अपराधीकरण रोकने के संदर्भ में आया सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला भी चर्चा के केंद्र में रहा। सभी राजनीतिक दलों ने एक सुर में सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से असहमति जताई है। जेल में बंद नेताओं को चुनाव नहीं लड़ने दिए जाने के राजनीतिक दुरुपयोग की चिंता सबको खूब सताई। कांग्रेस, भाजपा, वाम दल, सपा, राजद समेत सभी राजनीतिक दलों ने चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से जल्द से जल्द जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन संबंधी विधेयक लाने की मांग की। सभी दलों में इन निर्णयों को लेकर चिंता है और सबने इस स्थिति का समाधान व संसद की सर्वोच्चता बरकरार रखने की मांग की है। संसद और विधायिका की सर्वोच्चता कायम रखने के लिए विधेयक लाने से भी किसी ने इंकार नहीं किया है। हो सकता है इसके लिए मानसून सत्र का समय भी बढ़ाया जाए। देखा जाए तो ४८०७ सांसदों/विधायकों में से १४६० के खिलाफ आपराधिक केस चल रहे हैं। यानी देश में कुल ३० प्रतिशत नेता दागी हैं। लोकसभा के ५४३ सांसदों में से १६२ (३० प्रतिशत) सांसदों पर आपराधिक केस चल रहे हैं जिसमें से ७६ यानी १४ प्रतिशत पर गंभीर मामलों के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। राज्यसभा की बात करें तो २३२ सांसदों में से ४० यानी १७ प्रतिशत पर आपराधिक केस दर्ज हैं जिनमें से १६ यानी ७ प्रतिशत पर गंभीर मामलों के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। वहीं देश के ४०३२ विधायकों में से १२५८ यानी ३१ प्रतिशत विधायकों पर आपराधिक केस दर्ज हैं जिनमें से १५ प्रतिशत पर गंभीर मामलों के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। निर्दलीय जीतने वाले ४२ प्रतिशत सांसदों/विधायकों पर आपराधिक केस दर्ज हैं। नेताओं का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से संसद के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लग जाएगा। यदि इसे कानून के रूप में परिवर्तित किया गया तो इसका दुरुपयोग निश्चित हैं। नेताओं की चिंता को यदि स्वाभाविक भी मान लें तो क्या संसद की सर्वोच्चता की खातिर कानून को ही समाप्त किया जाना उचित है? क्या जनप्रतिनिधियों ने सर्वोच्च न्यायालय को पंगु करने का अघोषित निर्णय सा ले लिया है। पिछले कुछ सालों में उजागर हुए तमाम घोटालों-घपलों के पीछे सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता को नकारा नहीं जा सकता। यहां तक कि जिन नेताओं को कभी सज़ा नहीं होती थी, सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें सज़ा देकर देश के जनमानस में कानून के प्रति आदर का भाव पुनः जागृत किया था। ऐसे में स्वार्थी नेता यदि सर्वोच्च न्यायालय के जनहितैषी फैसलों को बहुमत के आधार पर बदलते रहेंगे तो यह देश की जनता के साथ अन्याय होगा। मानसून सत्र में भले ही दोनों प्रस्तावों को नकारकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को कुंद कर दिया जाए किन्तु जनता सब देख-समझ रही है। हो सकता है इसका हिसाब वह समय आने पर चुकता कर ले?