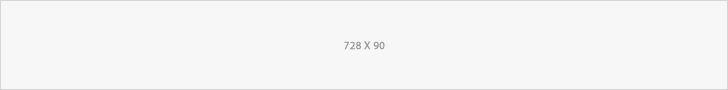सत्कर्म द्वारा लोगों को सुखी बनाना अच्छी बात है, लेकिन उससे कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। यही कर्म का मर्म है। स्वामी विवेकानंद के सार्धशती वर्ष में उनके स्मृति दिवस पर उनका ही चिंतन..
सत्कर्म द्वारा लोगों को सुखी बनाना अच्छी बात है, लेकिन उससे कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। यही कर्म का मर्म है। स्वामी विवेकानंद के सार्धशती वर्ष में उनके स्मृति दिवस पर उनका ही चिंतन..
भिन्न परिस्थितियों में कर्तव्य भिन्न-भिन्न हो जाते हैं। जो कार्य एक अवस्था में नि:स्वार्थ होता है, वही किसी अन्य अवस्था में स्वार्थपरक भी हो सकता है। किसी कार्य की कर्तव्य-अकर्तव्यता देश, काल और पात्र पर ही निर्भर करती है। एक देश में कोई आचरण नीतिसंगत माना जाता है, परंतु संभव है, वही किसी दूसरे देश में नीतिविरुद्ध हो। समस्त प्रकृति का अंतिम ध्येय मुक्ति है और यह मुक्ति केवल पूर्ण नि:स्वार्थता द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक स्वार्थशून्य कार्य, नि:स्वार्थ विचार, नि:स्वार्थ वाक्य हमें इसी ध्येय की ओर ले जाता है और इसीलिए हम उसे नीतिसंगत कहते हैं।
यह व्याख्या प्रत्येक धर्म एवं नीतिप्रणाली में लागू होती है। यदि तुम उन धर्म-संप्रदायों के किसी व्यक्ति से पूछो कि हमें अमुक कार्य क्यों करना चाहिए, तो वह उत्तर देगा कि ईश्वर की ऐसी ही आज्ञा है। उनके नीतितत्व का मूल चाहे जो हो, पर उसका सार यही है कि ‘वयं’ की चिंता न करो और ‘अहं’ का त्याग करो। परंतु जो लोग अपने क्षुद्र व्यक्तित्व से जकड़े रहना चाहते हैं, उनसे हम पूछें कि जरा ऐसे पुरुष की ओर देखो, जो नितांत नि:स्वार्थ हो गया है, जो स्वयं के लिए कोई भी कार्य नहीं करता और फिर बताओ कि उसका ‘निजत्व’ कहां है? जब तक वह अपने स्वयं के लिए विचार करता है, कोई कार्य करता है या कुछ कहता है, तभी तक उसे अपने निजत्व का बोध रहता है। परंतु यदि उसे केवल दूसरों के संबंध में ध्यान है, जगत के संबंध में ही ध्यान है, तो फिर उसका निजत्व भला कहां रहा? उसका तो सदा के लिए लोप हो चुका है।
अतएव कर्मयोग, नि:स्वार्थपरता और सत्कर्म द्वारा मुक्ति लाभ करने की एक विशिष्ट प्रणाली है। कर्मयोगी को किसी भी प्रकार के धर्ममत का अवलंबन करने की आवश्यकता नहीं। वह ईश्वर में भी विश्वास करे या न करे, आत्मा के संबंध में भी अनुसंधान करे या न करे, किसी प्रकार का दार्शनिक विचार भी करें अथवा न करें, इससे कुछ बनता-बिगड़ता नहीं। उसके जीवन का प्रत्येक क्षण ही मानो प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए, क्योंकि उसे अपनी समस्या का समाधान केवल कर्म द्वारा ही करना होता है।
संसार के प्रति उपकार करने का क्या अर्थ है? संसार के प्रति ऐसा कोई भी उपकार नहीं किया जा सकता, जो चिरस्थायी हो। हम किसी मनुष्य की भूख अल्प समय के लिए भले ही शांत कर दें, परंतु बाद में वह फिर भूखा हो जाएगा। किसी व्यक्ति को हम जो भी कुछ सुख दे सकते हैं, वह क्षणिक ही होता है। सुख और दुख रूपी इस सतत होने वाले रोग का कोई भी सदा के लिए उपचार नहीं कर सकता। इस सतत गतिमान सुख-दुख रूपी चक्र को कोई भी चिरकाल के लिए रोक नहीं सकता। क्या हमें सदैव से ही सुख-दुख, हर्ष-विषाद तथा अधिकार का तारतम्य पग-पग पर नहीं दिखाई देता? क्या कुछ लोग अमीर तो कुछ गरीब, कुछ बड़े तो कुछ छोटे, कुछ स्वस्थ तो कुछ रोगी नहीं हैं? यह दशा सदैव रही है, परंतु सुख-दुख की अनिवार्य भिन्नता के होते हुए भी उसे घटाने के प्रयत्न भी सदैव होते रहे हैं। इतिहास के प्रत्येक युग में ऐसे हजारों स्त्री-पुरुष हुए हैं, जिन्होंने दूसरों के जीवन-पथ को सुगम बनाने के लिए अविरत परिश्रम किया। पर वे कभी इसमें पूर्णत: सफल न हो सके। हम तो केवल एक गेंद को एक जगह से दूसरी जगह फेंकने का खेल खेल सकते हैं। हमने यदि शरीर से दुख को निकाल बाहर किया, तो वह मन में जा बैठता है। हम संसार के सुख को नहीं बढ़ा सकते। हम उसे सिर्फ यहां से वहां और वहां से यहां धकेलते रहते हैं। यह ज्वार-भाटा, यह चढ़ाव-उतार तो संसार की प्रकृति ही है। इसके विपरीत तो वैसा ही युक्तिसंगत होगा, जैसा यह कहना कि मृत्यु बिना जीवन संभव है। ऐसा कहना निरी मूर्खता है, क्योंकि जीवन कहने से ही मृत्यु का बोध होता है और सुख कहने से दुख का। यदि तुम्हें जीवन की अभिलाषा हो, तो उसके लिए तुम्हें प्रतिक्षण मरना होगा। जीवन और मृत्यु एक ही तरंग के उत्थान और पतन हैं। एक व्यक्ति पतन को देखता है और निराशावादी बन जाता है, दूसरा उत्थान देखता है और आशावादी बन जाता है।
कर्म प्रकृति की नींव का अंश है और सदैव चलता रहता है। जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, वे इसे अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ईश्वर असमर्थ पुरुष नहीं है, जिन्हें सहायता की आवश्यकता पड़े। हमारा ध्येय मुक्ति है, नि:स्वार्थता हमारा लक्ष्य है और उस ध्येय की प्राप्ति कर्म द्वारा ही करनी होगी। कर्मयोगी कहते हैं कि तुम्हें कर्म करने के लिए मुक्ति को छोड़ अन्य कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सब प्रकार के उद्देश्य के अतीत हो जाओ। कर्मफल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। जो स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से भी सत्कर्म करता है, वह भी अपने को बंधन में डाल लेता है।