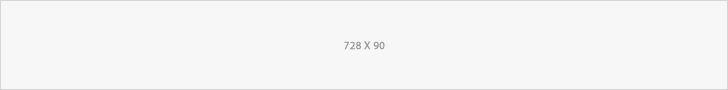सुमन मिश्र
नई दिल्ली- होली के त्यौहार को भक्त प्रह्लाद, हिरण्यकश्यपु और होलिका की कहानी से जोड़ा जाता है, जिसमें अन्य कहानियों की तरह ही असत्य पर सत्य की विजय होती है। लेकिन होली का एक आध्यात्मिक स्वरूप सूफियों और संतों के यहां भी मिलता है, जहां अपने आपको फना करके अपने ऊपर मुर्शिद या गुरु का रंग चढ़ाना और दुई का भेद खत्म होने का जश्न मनाया जाता है।
सूफियों और संतों के काव्य और उपदेश इस रंग में डूबे हुए हैं। यहां होली खुदी के मिट जाने का उत्सव है और परमात्मा के मिलन का नृत्य। तभी हजरत अमीर खुसरो इस रंग को महा रंग कहते हैं :
“आज रंग है री महा रंग है
मेरे महबूब के घर रंग है री।
मोहे पीर पायो निजामुद्दीन औलिया
जहां देखूं मोरे संग है री।”
अमीर खुसरो ने हिंदुस्तानी संस्कृति का रंग ओ गुलाल अपने कलाम में जमकर उड़ाया है। उन्होंने सूफियों को पहले पहल रंग दिया और हिंदुस्तानी तहजीब ने इस रंग को रंगरेज बना दिया। यह रंग उनके बाद के तमाम सूफियों और संतों के कलाम में ऱक्स करता नजर आता है।
खुसरो के तुरंत बाद ही विद्यापति ने प्रेम रस और श्रंगार रस को अपनी कविताओं में घोलकर घर-घर पहुंचाया। अब हिंदू और मुस्लमान दोनों पर धीरे-धीरे एक दूसरे का रंग चढ़ने लगा था और एक गंगा-जमुनी तहजीब का रंग तैयार होने लगा था। राजनीतिक उथल-पुथल से भरे इस दौर में भी सूफियों और संतों ने अपना यह रंग जमकर लुटाया। कबीर ने तो हद और अनहद दोनों रंग दिए। जब यह रंग चला तो कबीर के पदों में भी पहुंचा :
“गगन मंडल बिच होरी मची है, कोई गुरु गम तें लखि पाई
सबद डोर जहं अगर ढरतु है, सोभा बरनि न जाई
फगुवा नाम दियो मोहिं सतगुरु, तन की तपन बुझाई
कहै कबीर मगन भइ बिरहिनि, आवागवन नसाई।”
होली खेलते-खेलते कबीर खुद फगुवा बन गए। जब बे-खुदी का यह आलम हो तो होरी का यह रंग आम लोगों पर कैसे न चढ़ता! रंगों का यह सफर अनोखा होता है। एक बार चढ़ गया, पक्का हो गया तो उतारे नहीं उतरता।
नया रंग समाज बर्दाश्त नहीं करता। कबीर को भी बर्दाश्त नहीं किया गया। कबीर को खत्म करके लोगों ने सोचा कि उन्होंने रंग को खत्म कर दिया, पर रंग तो अपने सफर पर कब का निकल चुका था। आगे यही रंग बुल्लेह शाह की काफियों में मिलता है :
“होरी खेलूंगी कहकर बिस्मिल्लाह
नाम नबी की रतन चढ़ी, बूंद पड़ी इल्लल्लाह
रंग रंगीली उही खिलावे, जो सखी होवे फना फील्लाह
होरी खेलूंगी कहकर बिस्मिल्लाह।”
काशी में कबीर और कसूर में बुल्लेह शाह, रंग का यह सफर अविरल अविराम था। बुल्लेह शाह से पहले यह रंग मीरा के पदों में दिखता है। मीरा अपने रंगों में अविनाशी तत्व मिलाकर सब रंगों को पक्का कर देती हैं। सब कुछ सहज हो जाता है :
“सहज मिले अविनाशी रे!”
मीरा के अविनाशी, होरी में साकार रूप धरकर फाग खेलते हैं। दिल ही ब्रज हो जाता है और दिल ही काशी। मीरा प्रभु के रंग में रंगी जब उचारती हैं तो रंग ही रंग झरते हैं। वृंदावन भी लाल हो जाता है। मीरा रंगों के ही माध्यम से जीवात्मा को सचेत भी करती हैं :
“फागुन के दिन चार रे, होली खेल मना रे
बिन करताल पखावज बाजे, अनहद की झंकार रे!
बिन सुर राग छतीसूं गावे, रोम रोम रण कार रे
सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे!”
शाह तुराब अली कलंदर ने होरी के पदों में अपने उसी अविनाशी महबूब की चिरौरी की है :
“अब की होरी का रंग न पूछो
धूम मची है बिंदराबन मा
श्याम-बिहारी चतुर खिलारी
खेल रहा होरी सखियन मा
मो का कहां वह ढूंढे पावै
मैं तो छुपी हूं ‘तुराब’ के मन मा।”
हजरत शाह नियाज बरेलवी ने भी अपने हिंदवी कलाम में होरी पर गीत लिखे हैं। सूफियाना रंग में रंगी उनकी लेखनी हमें तसव्वुफ के गहरे रंगों से सराबोर कर देती है :
“होरी होय रही अहमद जियो के द्वार
नबी अली को रंग बनो है हसन हुसैन खिलार
ऐसो अनोखो चतुर खिलाड़ी रंग दीनो संसार
‘नियाज’ प्यारा भर भर छिड़के एक ही रंग पिचकार।”
सूफी प्रेमाख्यानक काव्य जब लिखे गए, तब उनका तानाबाना भी हिंदुस्तानी संस्कृति के धागे से ही बुना गया। फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को होली जलाना और दूसरे दिन उस जली हुई होली की राख उड़ाना तथा रंग और अबीर खेलना इस पर्व के लोकाचार थे।
‘पद्मावत’ में फाग खेलने, होली जलाने और झोली में राख लेकर उड़ाने की प्रथा का उल्लेख मिलता है :
“फाग खेलि पुनि दाहब होली, सें तब खेह उड़ाउब झोली।”
होली को शाहजहांनी काल के दौरान ईद-ए-गुलाबी और आब-पाशी भी कहते थे। कहते हैं कि मुगलिया हिंदुस्तान एक समय होली में अबीर ओ गुलाल से रंग जाया करता था। रंगों का यह जादू बादशाह-ए-व़क्त पर भी सर चढ़कर बोला। बादशाह बहादुरशाह जफर होली पर रंग और गुलाल लगवाते थे।
अठारहवीं सदी में भक्ति आंदोलन की एक लहर-सी चली, जिसमें कई निगुर्णी संत हुए जिनके कलाम सौभाग्य से उपलब्ध हैं। इनमे प्रमुख हैं- गुलाल साहेब, तुलसी साहेब (हाथरस वाले), भीखा साहेब आदि जिनकी वाणियों में होली के पद भी मिलते हैं :
“कोउ गगन में होरी खेलै
पांच पचीसो सखियां गावहिं बानि दसौ दिसि मेलै
अबकी बार फाग दीजै प्रभु जान देवै नहिं तौ लै
कहै ‘गुलाल’ कृपाल दयानिधि नाम दान दै गैलै।- गुलाल साहेब।
बाराबंकी में स्थित देवा शरीफ में हर साल होली मनाई जाती है। यह हिंदुस्तान की एकमात्र ऐसी दरगाह है, जहां होली का पर्व मनाया जाता है।
रंगों का कोई मजहब नहीं होता, न ही रंगों की कोई जात होती है, पर जब यही रंग अपने सफर पर निकलते हैं तो इंसान के भीतर कुछ जिंदा हो उठता है। रंगों का यह सफर जितना जाहिरी है।