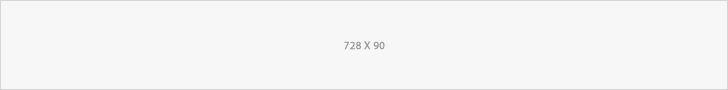इसमें दो राय नहीं कि भारतीय मीडिया का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है. इसके चरित्र से हर कोई वाकिफ है. लोकतंत्र पर नजर रखने वाले मीडिया की धार में भोथरापन आ चुका है और जो तेजी दिखती है, उसमें बाजारवाद है. बाजार को देखकर खबरों को परोसना और उसे बेचना इसकी फितरत बन गई है. समाज का आईना, आज साफ नहीं दिखता बल्कि, समाज को राह दिखाने वाला मीडिया समाज से दूर होता जा रहा है. खास तौर पर, सामाजिक न्याय के मसले पर, ये पूरी तरह से दूर हो चुका है. अब 13 सितंबर 2013 के दिन को ही लें. फैसले के दिन के रूप में हो हल्ला करने वाला मीडिया. बाजार देख तेजी से पलटा.
इसमें दो राय नहीं कि भारतीय मीडिया का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है. इसके चरित्र से हर कोई वाकिफ है. लोकतंत्र पर नजर रखने वाले मीडिया की धार में भोथरापन आ चुका है और जो तेजी दिखती है, उसमें बाजारवाद है. बाजार को देखकर खबरों को परोसना और उसे बेचना इसकी फितरत बन गई है. समाज का आईना, आज साफ नहीं दिखता बल्कि, समाज को राह दिखाने वाला मीडिया समाज से दूर होता जा रहा है. खास तौर पर, सामाजिक न्याय के मसले पर, ये पूरी तरह से दूर हो चुका है. अब 13 सितंबर 2013 के दिन को ही लें. फैसले के दिन के रूप में हो हल्ला करने वाला मीडिया. बाजार देख तेजी से पलटा.
दिल्ली छात्रा दुष्कर्म के दोषियों को अदालत सजा सुनाने वाली थी. मीडिया सुबह से ही इस खबर पर जमा थी. चर्चाओं का दौर चल रहा था. दोपहर में दोषियों को फांसी की सजा सुना दी गई. चैनलों पर गहमा-गहमी दिखी. लेकिन कुछ ही घंटे में खबरिया चैनलों का रुख बदल गया. भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मादी के नाम की घोषणा पर खबर फोकस हो गई. घोषणा के पहले और पूर्व में चैनलों पर जो कुछ दिखा उससे यही लगा कि मोदी को लेकर खबरिया चैनल वनडे क्रिकेट मैच खेल रहे हों ! समाज के लिए शर्मनाक ‘‘महिला दुष्कर्म की घटना’’ पर महत्वपूर्ण फैसले की खबर गौण होती दिखी. प्रिंट मीडिया ने भी कमोबेश वही किया, जो खबरिया चैनलों ने किया. दुष्कर्म की सजा की तुलना में ‘नमो’ की खबर को प्राथमिकता दी. जबकि खबर दो कॉलम के लायक थी. यही नहीं खबर को पहले पन्ने और अलग से पूरा पृष्ठ दिया गया. ऐसे में अन्य खबरें मीडिया में जगह पाने से वंचित रही.
सामाजिक न्याय की अवधारणा या संकल्पना समाज में एक आदर्श स्थिति की उद्घोषणा है. जिसका अर्थ है-समाज में सभी व्यक्ति समान समझे जाएंगे तथा व्यक्ति और व्यक्ति में जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, संपत्ति या अन्य किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा. भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार और कर्तव्य सामाजिक न्याय के ही मौन समर्थन हैं, जिसके तहत अस्पृश्यता, छुआछूत जैसी कृत्रिम सामाजिक बुराइयों की समाप्ति के स्पष्ट उल्लेख हैं.
देखा जाए तो भारतीय मीडिया सामाजिक मुद्दें व सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने में कोई खास भूमिका में खड़ी नहीं दिखती, जब तक कि कोई बड़ी घटना न हो. सामाजिक मुद्दा पर राजनीतिक मुद्दा हावी हो जाता है. बल्कि कर दिया जाता है. अगर हम पीछे देखेंगे तो पाएंगे कि ऐसे कई मामले हैं, जिसे मीडिया ने उठाया ही नहीं. उठाया भी तो हल्के ढंग से. पिछले ही दिनों आरक्षण के सवाल पर मीडिया पूरी तरह से बंटा दिखा. आरक्षण के समर्थन में मीडिया के स्वर प्रखर नहीं थे. आरक्षण के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों के लिए यह हां में हां मिलाता दिखा, उनकी खबरों को प्राथमिकता मिली. जो समर्थन में आवाज उठाते थे, उन्हें वह गोल कर देता है. जबकि जरूरत है विमर्श चलाने की. समाज के हालात क्या हैं, यह कोई छिपा कर रखनेवाली बात नहीं है. वर्षों बाद भी सामाजिक असामनता बरकरार है. बराबरी और गैर-बराबरी का फासला इतना बड़ा है कि इसे पाटना बड़ी बात है. मीडिया सामाजिक असमानता को पाटने में आगे बढ़ता नहीं दिखता, इसके उदाहरण भरे पड़े हैं.
सामाजिक न्याय की अवधारणा या संकल्पना समाज में एक आदर्श स्थिति की उद्घोषणा है. जिसका अर्थ है-समाज में सभी व्यक्ति समान समझे जाएंगे तथा व्यक्ति और व्यक्ति में जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, संपत्ति या अन्य किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा. भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार और कर्तव्य सामाजिक न्याय के ही मौन समर्थन हैं, जिसके तहत अस्पृश्यता, छुआछूत जैसी कृत्रिम सामाजिक बुराइयों की समाप्ति के स्पष्ट उल्लेख हैं. वस्तुतः सामाजिक न्याय का उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के साथ-साथ समानता प्रदान करना भी है. सभी नागरिकों को शिक्षा के समान अवसर की उपलब्धता और देश के प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों के समाज के सभी लोगों के बीच न्यायोचित वितरण की हिमायत ही सामाजिक न्याय का आईना है.
किसी भी प्रजातांत्रिक देश का सबसे उपयुक्त दस्तावेज ‘संविधान‘ होता है जिसमें मानव हितों के तमाम प्रावधान मौजूद होते हैं. लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के 66 वर्षों के बाद भी हमारे समाज में वैसी तमाम विसंगतियां मौजूद हैं, जो सामाजिक न्याय की, समतामूलक समाज की, समाजवादी राज्य की संकल्पना पर हर दिन कालिख पोत रही है. जातियों-उपजातियों में बंट चुका और बंट रहा समाज सिसक रहा है. आरक्षण के सरकारी प्रावधानों के बावजूद, आरक्षित वर्ग का सम्मान के साथ उत्थान सपने की तरह लगता है. आरक्षित वर्ग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर अनारक्षित यानी ऊंची जातियों के व्यंग्यात्मक बाणों को सहते रहने के लिए विवश है. दलित वर्ग अपने हक से वाकिफ नहीं है और सामाजिक क्रांति की एक हल्की कोशिश भी जन्म के पहले भी कुचल दी जाती है. दलितों के मंदिर प्रवेश पर प्रतिबंध की खबरें सारे देश के हिस्सों से आती रहती है. मानवीय मूल्यों का पतन रोजमर्रा की एक आम घटना हो गई है. आज आत्मकेंद्रित हो चुका समृद्ध वर्ग वैयक्तिक ऐश्वर्य की तलाश में राष्ट्र के सांस्कृतिक श्रृंगार को भुल चुका है. विज्ञान नए-नए अनुसंधानों के बल पर नित नई ऊंचाइयां छू रहा है और वर्तमान समाज जाति व्यवस्था की जकड़न में दिन-ब-दिन जड़ होता जा रहा है.
सवाल उठता है कि इसके लिये जिम्मेदार कौन है? इससे भी बड़ा और प्रासंगिक प्रश्न यह है कि सामाजिक समरसता की जवाबदेही किनके कंधों पर है? व्यस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या सामूहिक रूप से तीनों पर या किसी और पर ? मोटे तौर पर, देश के संतुलित, सम्यक और समावेशी विकास के लिए नियमों का सृजन व्यवस्थापिका के अधीन है और स्थापित नियमों का कार्यान्वयन कार्यपालिका का दायित्व है. न्यायपालिका की पैनी नजर होती है-दोनों ही अंगों पर ताकि दायित्वों का पूरा-पूरा निर्वहन हो और अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन न हो.
मीडिया को समाज के हर वर्ग, विशेषकर ग्रामीण, पिछड़े, गरीब वर्ग की मूल समस्याओं पर फोकस करने की अपनी भूमिका को ईमानदारीपूर्वक निभानी होगी. केवल बाजार को देख मुद्दे तय नहीं होने चाहिए. मुद्दों को बराबर जगह दिए जाने की जरूरत है.
आजादी के बाद से ही नए रचनात्मक क्रियाकलापों और राष्ट्र हित में कर्तव्यों के परिपालन में पत्रकारिता की एक ठोस, सार्थक और सबल भूमिका रही है. दरअसल लोकतांत्रिक प्रशासन का एक अपरिहार्य अंग मीडिया है, जो चौथे खंभे के तौर पर जाना जाता है. इसकी जवाबदेही लोकत्रंत के अन्य खंभों से ज्यादा महवपूर्ण है. इस चौथे खंभे से हमेशा ही पूरे देश की अनगिनत उम्मीदें बंधी होती हैं और उन उम्मीदों पर यथासंभव खरा उतरना मीडिया की सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी होती है. राष्ट्रहित और जनहित में बिना किसी भेदभाव के समाज की हर हलचल को शब्दों में पिरोना ही पत्रकारिता है. समाज के हर वर्ग की आकांक्षाओं को गुंजित करना पत्रकारिता की मर्यादा है. समाज के हर वर्ग के सपनों की हिफाजत और किसी के प्रति, किसी भी तरह की ज्यादती के विरोध में सशक्तता से खरा होना ही मीडिया का यथार्थ संदर्भ है.
अब सवाल है कि अगर किसी लोकतांत्रिक देश के किसी भी कोने में किसी एक व्यक्ति या समूह के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति या समूह पर अमानवीय कृत्य बार-बार होता है, इस तरह की कृतियों से अगर मानवता का चेहरा बार-बार लहूलुहान होता है, तो व्यापक दायरे और विशाल दायित्व वाले मीडिया पर शायद इस खून के छींटे सबसे पहले पडते हैं और पड़ने भी चाहिए. इसे न सिर्फ सामाजिक न्याय की परिभाषा के अक्षर मिटते हैं बल्कि मीडिया को लेकर स्थापित वर्जनाएं भी टूटती हैं. जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आशीष नंदी के बयान के बाद दलित-पिछड़ों के आक्रोश और मीडिया द्वारा नंदी के बचाव की कोशिश ने मीडिया पर से पिछड़े-दलितों के विश्वास की परतों को खरोचने का ही काम किया है. आखिर, इसकी वजहें क्या हैं? क्यों ऐसा ही बार-बार होता है? और कैसे और कहां इसके समाधान की तलाश की जा सकती है?
मीडिया को समाज के हर वर्ग, विशेषकर ग्रामीण, पिछड़े, गरीब वर्ग की मूल समस्याओं पर फोकस करने की अपनी भूमिका को ईमानदारीपूर्वक निभानी होगी. केवल बाजार को देख मुद्दे तय नहीं होने चाहिए. मुद्दों को बराबर जगह दिए जाने की जरूरत है. हालांकि मीडिया का इनसे दूरी बढ़ाता जा रहा है. इसकी वजह साफ है कि उसकी नजर में वहां बाजार नहीं है. देखा जाए तो जब तक कोई बड़ी घटना नहीं घटती, सामाजिक न्याय के मुद्दा खबर नहीं बनते हैं और बनती भी है तो सही तस्वीर मीडिया में नहीं आती है. खबर आ भी जाती, तो जानबूझकर खबरों को अंदर के पेज में दिया जाता है. ताकि लोगों की नजर नहीं पड़े. आज भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वालों के साथ मीडिया का व्यवहार दोयम दर्जे का है. ऐसे में मीडिया का सवालों के घेरे में आना स्वाभाविक है.
साभार गुलेल डॉट कॉम