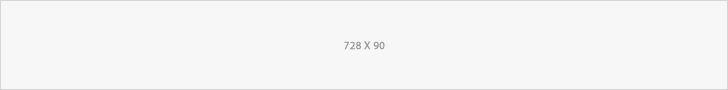हिन्दी पट्टी हिंसा, बाजार और सांप्रदायिकता से इतना कभी नहीं घिरी. नफरत के कुएं में भाषा, विचार, तहजीब, मनुष्य- सब गिराए जा रहे हैं. फरेब और झपट का बोलबाला है. ये हिन्दी भाषा का अपने समाज से बड़े अलगाव का समय है.
हिन्दी पट्टी हिंसा, बाजार और सांप्रदायिकता से इतना कभी नहीं घिरी. नफरत के कुएं में भाषा, विचार, तहजीब, मनुष्य- सब गिराए जा रहे हैं. फरेब और झपट का बोलबाला है. ये हिन्दी भाषा का अपने समाज से बड़े अलगाव का समय है.
ऐसे समय में जब सरकारी गैर सरकारी ठिकानों में 14 सितंबर यानी हिन्दी दिवस जोरशोर से मनाया जाता है तो न जाने क्यों दुर्गंध उठती है. मानो कुछ आग के हवाले किया जा रहा है. कोई अजीबोगरीब यज्ञ हो और आहुतियां दी जा रही हों. संदेह और घृणा भरे ऐसे हालात हैं. हिन्दी दिवस औपचारिकता और नाटकीयता तो बन ही गया था, अब ये खोखला भी हो चुका है. इसके दरवाजे गीले हो चुके हैं, खिड़कियां गिरने को हैं, दीवारें हिल गई हैं और दीमकें जैसे इस जर्जरता में आखिरी सूराख करती बढ़ रही हैं. हिन्दी अपने दिवस की भव्यता में गठरी तो बनी ही रहती थी अब लगता है ढेर भी वहीं हो जाएगी.
सबसे पहले कट्टर व्याकरणवादियों और शुद्धतावादियों ने हिन्दी को कैद किया. संस्कृत भाषा के आदिगुरू पाणिनी ने अष्टाध्यायी में लिख दिया था, “व्याकरण भाषा का कंकाल है, उसकी आत्मा नहीं.” पाणिनी तो छोड़िए हम तो अपने समय के विद्वानों की भी नहीं सुनते. भवानीप्रसाद मिश्र ने कहा था, “जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख/ और उसके बाद भी हम से बड़ा तू दिख”. लेकिन किसे फुरसत है. ये हिन्दी तो अफसरी ठाठबाट में अघाती, सुस्ताती, सजी संवरी, बनीठनी सी रहती है. जैसा रघुबीर सहाय ने अपनी एक कविता में बताया थाः
हमारी हिन्दी एक दुहाजू की नई बीवी है
बहुत बोलनेवाली बहुत खानेवाली बहुत सोनेवाली
गहने गढ़ाते जाओ
सर पर चढ़ाते जाओ….
सरकार और साहित्य से लेकर शिक्षा तक फैला, उसका अमला ऐसी ही हिन्दी चाहता है. उस सरकारी भाषा को देखकर आप कांप जाते हैं. क्या वो हिन्दी है या उसके भेस में क्रूरता. दूसरी तरफ हिन्दी एक ऐसी भाषा है जो राजसी ठाठबाट की दिशा में अग्रसर एक शातिर लफंगई के हवाले से आती है. वो अक्सर षडयंत्र करने वाली भाषा बन जाती है- अपनी मिट्टी अपने जन और अपनी संस्कृति से. वह जैसे अपने ही लोगों की जासूसी करती है. जो लोग हिन्दी को एक उन्मुक्त उड़ान देना चाहते हैं, उनके बारे में दरबार के कान भरती रहती है कि भाई देखो ये हिन्दी को महल में आने से रोकने वाले लोग हैं. इन्हें पकड़ो. हिन्दी का अंग्रेजीकरण करने वाला तबका भी यही है. वो हिन्दी को अंग्रेजी की तरह बोलता है और इस तरह अपने समाज से दूर रहता है.
अब सवाल ये है कि हमारी हिन्दी कहां गई. दिवस की लाली की ओट में छिपी वह हिन्दी तो हमारी नहीं या वही हिन्दी है, जिसे अगवा कर वहां उन चमकीले पर्दों के पीछे पहुंचा दिया गया है. उनमें से एक पर्दा बाजार का होगा. हमारे पास जो भाषा रह गई है, वो हमें प्रपंच, हिंसा और लड़ाई के लिए उकसाती है. मिसाल के लिए “मुझे मत मारो” की भावना व्यर्थ कर दी गई है और “मार डालो” की हुंकार से भाषा का पूरा घड़ा भर दिया गया है. हिन्दी में शायद यही पाप का घड़ा हो. पर ये भरता क्यों नहीं. क्यों.
अपनी हिन्दी की फिक्र इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि मनुष्य के तौर पर हम अपनी भाषा से दूर जा रहे हैं. हमारे व्यवहार और हमारे व्यक्तित्व में जो कालापन आ रहा है, खुराफातें बढ़ रही हैं और इतनी विमुखता आ गई है, वो भाषा से हमारा नैतिक और मानवीय संपर्क टूट जाने का नतीजा है. हमारा भाषा संस्कार प्रदूषित हो चुका है. यहां तक कि “नमस्ते” भी हम दिल से नहीं कह पाते. इतने दूर हम खुद से हो गए हैं.
अब जरा हिन्दी के मीडिया को भी देखें. भाषा की मिठास, आवेग और गंभीरता को तो उसने सबसे पहले छोड़ा. प्रयोग के नाम पर एक विकृत भाषाई माहौल बनाया. हिन्दी वाले हीनताबोध में और इस चक्कर में पैदा हुई वीरता के प्रभाव में ऐसी हिन्दी बोलते, गढ़ते हैं जो वास्तविक भाषा तो है ही नहीं. अपने मीडिया में हम ये अक्सर देखते हैं, जहां रूपक, अलंकार, विशेषण और उपमाएं झाग की तरह बहने लगती हैं. वे स्वाभाविक और सहज ढंग से बोल ही नहीं पाते. न जाने क्या बात है. किसने उनके मुंह में वैसी भाषा ठूंस दी है. ये झाग हिन्दी का नहीं हो सकता.
भाषाई पहलवानी का एक नमूना ये भी देखिए जो पिछले दिनों की एक खबर का इंट्रो हैः
विश्व प्रसिद्ध ऑर्केस्ट्रा संचालक जुबिन मेहता ने शाम को डल झील के तट पर स्थित शालीमार बाग में कुछ सर्वाधिक लोकप्रिय और पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत की सर्वश्रेष्ठ भावपूर्ण धुनों को जब जबरवान हिल्स की शानदार पृष्ठभूमि में छेड़ा तो श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए।
इस वाक्य को लपेटकर हिन्दी दिवस में जाएंगें. और क्या कहें. असल में बात सिर्फ हिन्दी को उसकी अकादमिक जटिलताओं और मक्कारियों से निकालने की ही नहीं है, ये नकली नारेबाजी और हिन्दी-विलाप रोकना होगा. जैसे प्रकाश झा का “सत्याग्रह”- न जाने कौन सी क्रांति का चमकीला और भारी भरकम रुदन. या फिर भाषाई बर्बरता का “रांझणा”.
हिन्दी की असली लड़ाई वहीं है जहां उसका जीवन और समाज है. पथरीली, ऊबड़खाबड़, धूल, खूनपसीने और आंसू से भरी जमीन. भाषाएं इसलिए नहीं मर जातीं कि हम उन्हें भूलते जाते हैं या उन्हें जीवन से निकाल देते हैं, वे इसलिए भी दम तोड़ने लगती हैं क्योंकि वे मनुष्यता को कुचलने का हथियार बना दी जाती हैं. जबकि उनका बुनियादी स्वभाव प्रेम, स्वप्न, उम्मीद, आकांक्षा और संघर्ष की हिफाजत का है. वे इंसानियत का निर्माण करती हैं.
हिन्दी ऐसी ही एक भाषा थी, है और रहेगी कहने पर न जाने क्यों अब संकोच और सवालिया निशान आ गया है. इसे आप विडंबना की तरह पढ़िए. या छटपटाहट की तरह.ब्लॉगः शिवप्रसाद जोशी