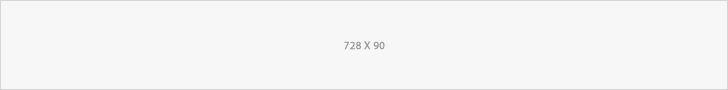उत्तराखंड के राजनीतिक संकट पर आए नैनीताल उच्च न्यायलय के फैसले ने सियासी गलियारों मंे राजनैतिक बेचैनी बढ़ा दी है। अदालत के इस फैसले ने एक बार फिर राजनीति और संवैधानिक अधिकारों को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। इस निर्णय के बाद सवाल यह उठ खड़ा हुआ है कि क्या संवैधानिक संस्थाओं की ओर से लिया गया फैसला गलत था?
उत्तराखंड के राजनीतिक संकट पर आए नैनीताल उच्च न्यायलय के फैसले ने सियासी गलियारों मंे राजनैतिक बेचैनी बढ़ा दी है। अदालत के इस फैसले ने एक बार फिर राजनीति और संवैधानिक अधिकारों को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। इस निर्णय के बाद सवाल यह उठ खड़ा हुआ है कि क्या संवैधानिक संस्थाओं की ओर से लिया गया फैसला गलत था?
अगर यह सच है तो इस तरह के फैसले क्यों लिए गए? नैतिक रूप से जहां कांग्रेस की जीत हुई है, वहीं केंद्र की मोदी सरकार इस फैसले पर कटघरे में खड़ी दिखती है।
केंद्र सरकार ने हालांकि नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन अदालत के फैसले और न्यायाधीश के दायित्वों पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। इस फैसले पर आशंकाएं पहले से ही उठ रही थीं। यह संवैधानिक कम, राजनैतिक निर्णय अधिक प्रतीत हो रहा था। इस मामले को लेकर अदालत ने महामहिम पर भी सवाल उठाया है।
अदालत ने कहा है कि राष्ट्रपति से भी गलती हो सकती है। अदालत ने पद की गरिमा बनाए रखते हुए परोक्ष रूप से सभी को कटघरे में खड़ा किया है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की दलीलों के तहत अनुच्छेद 356 के प्रयोग को गलत बताते हुए रावत सरकार को बहाल करने का फैसला सुनाया है।
अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या आदेश देती है। सभी की निगाहें उसी पर टिकी हैं। उधर, कांग्रेस के नौ बागी विधायकों की कुर्सी भी खतरे में हैं। अदालत ने उन्हें भी अयोग्य घोषित किया है। अगर देश की सर्वोच्च अदालत इस फैसले पर मुहर लगा देती है तो सियासी खेल की सारी गणित बेकार हो जाएगी। बागियों की बादशाहत भी किसी काम की नहीं रह जाएगी।
नैनीताल उच्च न्यायालय ने रावत सरकार को 29 अप्रैल को बहुमत सिद्ध करने का आदेश दिया है। जस्टिस के.एफ. जोसेफ ने अपने फैसले में कहा है कि किस आधार पर राज्य को राष्ट्रपति शासन के हवाले किया गया? राज्यपाल की ओर से राष्ट्रपति को भेजी गई रिपोर्ट में भी इस तरह का कोई जिक्र नहीं है, जिससे यह माना जाए कि राज्य में संवैधानिक संकट है।
राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने में केंद्र सरकार ने जिस उतावलेपन का परिचय दिया था, उसे उचित नहीं कहा जा सकता। सरकार सदन में अपना बहुमत सिद्ध कर पाती, इससे पहले ही राज्य को राष्ट्रपति शासन के हवाले कर दिया गया। यह संवैधानिक रूप से लाजिमी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राज्य में हरीश रावत सरकार लोकतांत्रित व्यवस्था के तहत चुनी हुई सरकार है।
राज्य में इसके पहले विजय बहगुणा मुख्यमंत्री थे। राज्यपाल ने रावत सरकार को सदन में 28 मार्च को बहुमत सिद्ध करने का समय दिया था, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल्दबाजी में जिस व्यवस्था को अपनाया, उसे कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। इसके पीछे क्या कारण थे, इसकी भी तस्वीर कुछ खास नहीं साफ नहीं दिखती। भाजपा ने उत्तराखंड के राजनीतिक हालात पर जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी दिखाई।
यह दीगर बात है कि कांग्रेस के नौ बागी विधायकों की ओर से सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद रावत सरकार अल्पमत में आ गई थी। लेकिन उसे अपना बहुमत साबित करने का मौका था।
सरकार अपना बहुमत न सिद्ध कर पाती, उस स्थिति में केंद्रीय मंत्रिमंडल राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता था। लेकिन बहुमत साबित करने के पहले ही सरकार को बर्खास्त किया जाना कहां की संवैधानिकता है? यह लोकतांत्रित मर्यादाओं का खुला उल्लंघन है।
यह कांग्रेस का आंतरिक संकट था। कांग्रेस इस संकट से चाहे जिस तरह से निपटती, यह उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य में प्रतिपक्षी भाजपा ने जिस तरह बागी विधायकों को संरक्षण दिया, उससे साफ जाहिर होता है कि उत्तराखंड सरकार को अपदस्त करने में भाजपा और बागियों की अहम भूमिका रही।
दूसरी बात, वक्त से पहले मोदी सरकार ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर यह साबित कर दिया था कि इस सियासी खेल में उसकी भी अहम भूमिका है। अंकों की बाजीगरी लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है।
मोदी सरकार का तर्क रहा कि बहुमत साबित करने के लिए अलोकतांत्रित तरीके अपनाए जा रहे थे। विनियोग विधेयक पारित नहीं हो सका था। विधायकों की ‘डील’ का एक कथित स्टिंग वीडिओ आने के बाद यह खुलासा हुआ था कि विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। हालांकि रावत ने इसे पूरी तरह फर्जी बताया था। लेकिन मोदी सरकार को एक बहाना मिल गया।
कांग्रेस के घरेलू झगड़े का सीधा लाभ उठाने में भाजपा कामयाब रही है। विजय बहगुणा और बागियों को आगे कर उसने जो राजनीतिक चाल चली, वह पूरी तरह कामयाब रही। राज्य में पार्टी को बिखरने से बचाने में सोनिया और राहुल गांधी नाकाम रहे हैं।
उत्तराखंड में जो कुछ हुआ, वह राजनैतिक लिहाज से कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। राज्य में बगावत की नींव तो उसी दिन पड़ गई थी, जिस दिन बहगुणा को हटाकर हरीश रावत को राज्य में सरकार चलाने को कहा गया था। ऐसी स्थिति में विजय बहगुणा और बागी वक्त के इंतजार में थे और मौका पाते ही उन्होंने अपना पासा फेंक डाला।
कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व पार्टी पर अपनी पकड़ खोता जा रहा है। कांग्रेस संसद में मोदी सरकार को शोरगुल से घेरने के बजाय अपने टूटते घर को पहले बचाए। वरना देश की सबसे बड़ी और पुराने राजनैतिक दल का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। संसद में 44 का आंकड़ा इसी तरफ इशारा करता है।
लेकिन उत्तराखंड में जो कुछ हुआ उसे पूरी तरह लोकतांत्रित नहीं कहा जा सकता। संख्या बल के कारण ही एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। यह लोकतांत्रित व्यवस्था के लिए सबसे खतरनाक जहर है।
बदलते राजनैतिक हालता के साथ इस कानून की भी समीक्षा होनी चाहिए। फिलहाल राज्य में राजनैतिक संकट अभी खत्म होने वाला नहीं है। लोकतंत्र की स्थिति बावली सी हो गई है।
हरीश रावत ने केंद्र सरकार के फैसले को राज्य के उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। रावत की दलील पर उन्हें 31 मार्च को विश्वासमत हासिल करने का आदेश दिया गया था, लेकिन उसी अदालत की युगलपीठ ने विश्वासमत पर रोक लगा दी थी।
अब नैनीताल उच्च न्यायालय ने केंद्र के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए राज्य में रावत सरकार को बहाल करने का आदेश दिया है।
उधर, अदालत ने बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने के विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के फैसले को सही ठहराया है। कुंजवाल ने नौ बागी विधायकों की सदस्यता खत्म कर दी थी। राज्यपाल की तरफ से रावत सरकार को 28 मार्च को बहुमत सिद्ध करने का समय दिया गया था। लेकिन इसके एक दिन पहले यानी 27 मार्च को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया।
अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। नैनीताल उच्च न्यायलय के फैसले के बाद भाजपा और मोदी सरकार कटघरे में खड़ी दिख रही है।
अदालत की ओर से की गई तल्ख टिप्पणी कई सवाल उठाती है। राष्ट्रपति की संवैधानिक गरिमा और निर्णय पर भी अदालत ने सवाल उठाए हैं। निश्चित तौर पर अदालत से बड़ा कोई नहीं हो सकता, यह भी सच है कि गलती हर इंसान से होती है।
दूसरी बात, ऐसी स्थिति जब बनती है तो राष्ट्रपति पर केंद्रीय राजनीति के दबाब का घेरा बन जाता है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश के बाद जो प्रस्ताव राष्ट्रपति के बाद गया हो, उस पर अधिक बहस उचित नहीं होती है।
हालांकि इस फैसले के लिए राष्ट्रपति उतने जिम्मेदार नहीं हैं, जितनी कि केंद्रीय सरकार और उसका मंत्रिमंडल। एक ही सवाल बार-बार उठता है कि सरकार को बहुमत साबित क्यों नहीं करने दिया गया। अब सर्वोच्च अदालत का फैसला आने के बाद ही स्थिति साफ होगी। लेकिन राज्य में दोबारा चुनाव ही सबसे बेहतर विकल्प होगा। (आईएएनएस/आईपीएन)
(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)